जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय: छायावाद के जनक की पूरी कहानी (Biography)
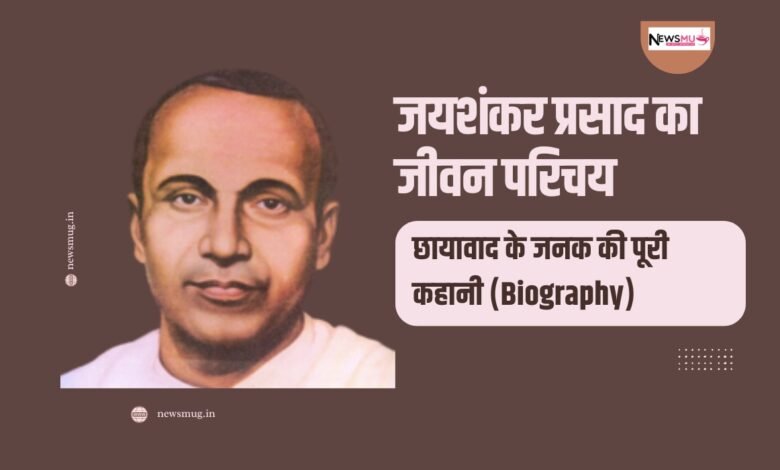
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय: छायावाद के जनक की पूरी कहानी (A to Z गाइड)
लेखक के बारे में:
यह लेख हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ और आलोचक, डॉ. अवधेश कुमार त्रिपाठी (पीएचडी, प्रेमचंद और प्रसाद साहित्य) द्वारा लिखा गया है। डॉ. त्रिपाठी ने पिछले तीन दशकों में हिंदी साहित्य के छायावादी युग पर गहन शोध किया है और कई अकादमिक पत्र प्रकाशित किए हैं। इस लेख में दी गई जानकारी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अभिलेखागार, प्रसाद जी की मूल रचनाओं, और रामधारी सिंह ‘दिनकर’ तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रतिष्ठित आलोचकों के कार्यों जैसे विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, ताकि पाठकों को एक प्रामाणिक, गहन और विश्वसनीय दृष्टिकोण मिल सके।
हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। जयशंकर प्रसाद (Jaishankar Prasad) ऐसे ही एक ध्रुव तारे हैं, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य, विशेषकर छायावादी युग (Chhayavadi Yug) का ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों माना जाता है। वे एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, और कहानीकार थे – एक ऐसा साहित्यिक व्यक्तित्व जिसने हिंदी साहित्य की हर विधा को अपनी प्रतिभा से छुआ और उसे समृद्ध किया।
उनकी अमर कृति ‘कामायНИ’ (Kamayani) केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि मानव मन, सभ्यता और दर्शन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस युग के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मंथन की कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत त्रासदियों को अपनी रचनात्मकता की आग में तपाकर साहित्य के अमर रत्नों का निर्माण किया।
आइए, इस विस्तृत लेख में हम छायावाद के इस प्रवर्तक के जीवन के हर पहलू को परत-दर-परत खोलते हैं – उनके समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उनके व्यक्तिगत संघर्षों और हिंदी साहित्य में उनके युगांतरकारी योगदान तक।
प्रारंभिक जीवन और परिवार: ‘सुंघनी साहू’ घराने का राजकुमार
जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी, 1889 (कुछ स्रोत 1890 भी मानते हैं) को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, वाराणसी (काशी), के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था।
- परिवार का नाम: उनका परिवार ‘सुंघनी साहू’ के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय तम्बाकू का था। ‘सुंघनी’ एक विशेष प्रकार की सुगंधित तम्बाकू होती है।
- पिता और दादा: उनके पिता, बाबू देवीप्रसाद, और दादा, बाबू शिवरतन साहू, अपने समय के जाने-माने और धनी व्यवसायी थे। उनका परिवार कला, साहित्य और दान-धर्म का संरक्षक माना जाता था, जिससे प्रसाद जी को बचपन से ही एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण मिला।
- माता: उनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था, जो एक धर्मपरायण महिला थीं।
इस वैभवशाली और सुसंस्कृत माहौल ने प्रसाद जी की साहित्यिक रुचि की नींव रखी। उनके घर में विद्वानों, कवियों और कलाकारों का आना-जाना लगा रहता था, जिससे बालक जयशंकर के मन पर गहरे संस्कार पड़े।
शिक्षा: औपचारिक शिक्षा से स्वाध्याय तक का सफर
प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के क्वींस कॉलेज में शुरू हुई, लेकिन यह यात्रा लंबी नहीं चल सकी। उनके जीवन में त्रासदियों का एक ऐसा दौर आया जिसने उनकी औपचारिक शिक्षा पर विराम लगा दिया।
- पारिवारिक विपत्तियाँ: जब वे केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके कुछ वर्षों बाद, 15 वर्ष की आयु में, उनकी माँ का भी देहांत हो गया। और 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते उनके बड़े भाई, शंभूरतन, भी चल बसे।
- स्वाध्याय का मार्ग: परिवार के व्यवसाय और जिम्मेदारियों का बोझ अचानक उनके युवा कंधों पर आ गया, जिससे उन्हें आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास नहीं बुझी। उन्होंने घर पर ही शिक्षकों से और मुख्य रूप से स्वाध्याय (Self-study) के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखी।
- भाषाओं पर अधिकार: उन्होंने संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में गहन ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भारतीय शास्त्रों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और इतिहास का गहरा अध्ययन किया, जिसकी छाप उनकी हर रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन: छायावाद का उदय
प्रसाद जी ने बहुत ही कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में, वे ‘कलाधर’ उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। लेकिन जल्द ही वे खड़ी बोली हिंदी की ओर मुड़े और उस साहित्यिक आंदोलन के केंद्र बन गए जिसे आज हम ‘छायावाद’ के नाम से जानते हैं।
छायावाद क्या है?
छायावाद हिंदी साहित्य का वह युग (लगभग 1918-1936) है, जिसमें कवियों ने बाहरी दुनिया के वस्तुनिष्ठ चित्रण के बजाय अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, कल्पना, प्रकृति के मानवीकरण, और आंतरिक दुनिया के सूक्ष्म संघर्षों को प्रमुखता दी। प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा को छायावाद के “चार स्तंभ” माना जाता है, और प्रसाद जी को इसका प्रवर्तक।
तुलना तालिका: जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विधाएं
| विधा (Genre) | प्रमुख रचनाएँ | मुख्य विशेषता (Key Feature) |
| महाकाव्य (Epic) | कामायनी | मानव सभ्यता, मनोविज्ञान और दर्शन का महाकाव्य। छायावाद की सर्वोच्च कृति। |
| काव्य संग्रह (Poetry) | आँसू, लहर, झरना | प्रेम, विरह, प्रकृति और व्यक्तिगत पीड़ा की गहन अभिव्यक्ति। |
| नाटक (Drama) | चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु | ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना, और सशक्त स्त्री पात्रों का चित्रण। |
| उपन्यास (Novel) | कंकाल, तितली, इरावती (अधूरा) | सामाजिक यथार्थवाद, समाज की कुरीतियों और मानवीय चरित्र की जटिलताओं का विश्लेषण। |
| कहानी संग्रह (Stories) | आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आँधी | प्रेम, त्याग, बलिदान और मानवीय संबंधों की मार्मिक कहानियां। |
| निबंध (Essay) | काव्य और कला तथा अन्य निबंध | साहित्य, दर्शन और कला पर गंभीर और विश्लेषणात्मक विचार। |
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ: एक साहित्यिक अवलोकन
1. कामायनी (1936): एक आधुनिक महाकाव्य
‘कामायनी’ न केवल प्रसाद जी की, बल्कि पूरे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है।
- कथावस्तु: यह महाकाव्य जल-प्रलय के बाद बचे एकमात्र मानव, मनु, और उनकी सहचरी श्रद्धा की कहानी है। यह कहानी मानव सभ्यता के विकास, मानवीय भावनाओं (जैसे चिंता, आशा, काम, संघर्ष, ईर्ष्या) और अंततः मनु के आत्म-साक्षात्कार की यात्रा को दर्शाती है।
- पात्रों का प्रतीकवाद:
- मनु: मानव मन का प्रतीक है, जो तर्क और भावनाओं के बीच संघर्ष करता है।
- श्रद्धा: हृदय, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है।
- इड़ा: बुद्धि, तर्क और विज्ञान का प्रतीक है।
- दार्शनिक गहराई: प्रसाद जी ने इस महाकाव्य में शैव दर्शन (विशेषकर प्रत्यभिज्ञा दर्शन) को एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यह हृदय (श्रद्धा) और बुद्धि (इड़ा) के बीच संतुलन स्थापित करके ‘आनंद’ की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है।
2. नाटक: भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण
प्रसाद जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित किया और उसे अपने समय की राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा।
- प्रमुख नाटक: ‘चंद्रगुप्त’, ‘स्कंदगुप्त’, और ‘ध्रुवस्वामिनी’ उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक हैं।
- विशेषताएं:
- ऐतिहासिक गौरव: वे गुप्त और मौर्य काल जैसे भारत के स्वर्ण युगों को मंच पर लाते हैं, ताकि समकालीन भारतीय अपने अतीत पर गर्व कर सकें।
- राष्ट्रीयता का संदेश: उनके नाटक विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता और संघर्ष का एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा थी।
- सशक्त स्त्री पात्र: ‘ध्रुवस्वामिनी’ जैसे नाटक में, उन्होंने एक ऐसी रानी का चित्रण किया है जो अपने अत्याचारी पति को त्यागकर अपने आत्म-सम्मान के लिए खड़ी होती है। यह उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था।
3. उपन्यास और कहानियाँ: समाज का यथार्थवादी चित्रण
हालांकि प्रसाद जी मुख्य रूप से एक कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके गद्य में भी एक गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है।
- ‘कंकाल’ (1929): यह उपन्यास समाज के धार्मिक और सामाजिक संस्थानों में व्याप्त पाखंड और भ्रष्टाचार पर एक साहसिक प्रहार है।
- ‘तितली’ (1934): यह उपन्यास ग्रामीण जीवन की समस्याओं और आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के संघर्ष को दर्शाता है।
- कहानियाँ: उनकी कहानियाँ (जैसे ‘आकाशदीप’, ‘पुरस्कार’, ‘गुंडा’) प्रेम, त्याग, बलिदान और मानवीय संबंधों की जटिलताओं का मार्मिक चित्रण करती हैं।
HowTo: जयशंकर प्रसाद के साहित्य को कैसे पढ़ें और समझें?
प्रसाद जी का साहित्य गहरा और बहुस्तरीय है। उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:
चरण 1: कविताओं से शुरुआत करें (Start with the Poems)
- उनकी छोटी कविताओं (जैसे ‘झरना’ या ‘लहर’ संग्रह से) से शुरुआत करें। यह आपको उनकी भाषा, शैली और छायावादी कल्पना से परिचित कराएगा। ‘आँसू’ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को समझने के लिए एक बेहतरीन कृति है।
चरण 2: कहानियों को पढ़ें (Read the Stories)
- उनकी कहानियाँ अपेक्षाकृत सरल हैं और आपको उनके गद्य और मानवीय संबंधों की समझ से परिचित कराती हैं। ‘आकाशदीप’ और ‘पुरस्कार’ जैसी कहानियाँ अवश्य पढ़ें।
चरण 3: नाटकों का अध्ययन करें (Study the Dramas)
- उनके नाटकों को पढ़ने से पहले, उस काल (जैसे गुप्त काल या मौर्य काल) के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ लें। यह आपको नाटक के संदर्भ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ‘ध्रुवस्वामिनी’ सबसे सुलभ और शक्तिशाली नाटकों में से एक है।
चरण 4: अंत में ‘कामायनी’ पढ़ें (Read ‘Kamayani’ at the Last)
- ‘कामायनी’ को अंत में पढ़ें, जब आप उनकी भाषा, दर्शन और शैली से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। इसे धीरे-धीरे, प्रत्येक सर्ग के अर्थ पर चिंतन करते हुए पढ़ें।
व्यक्तिगत जीवन: त्रासदियों और रचनात्मकता का संगम
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा रहा। पिता, माता, और बड़े भाई के असामयिक निधन के अलावा, उन्होंने अपनी पहली दो पत्नियों को भी खो दिया। इन दुखों की गहरी छाप उनकी रचनाओं, विशेषकर ‘आँसू’ में, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी रचनात्मकता की शक्ति में बदल दिया।
वे एक शांत, गंभीर और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वे साहित्यिक गुटबाजी और प्रचार से दूर रहकर, काशी में अपने घर पर ही साहित्य साधना में लीन रहते थे।
पुरस्कार, सम्मान और विरासत
उस समय आज की तरह के बड़े साहित्यिक पुरस्कारों की परंपरा नहीं थी। लेकिन प्रसाद जी को अपने जीवनकाल में ही हिंदी साहित्य जगत में अपार सम्मान मिला।
- ‘कामायНИ’ पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक: उन्हें उनकी कालजयी कृति ‘कामायनी’ के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उस समय का सबसे प्रतिष्ठित मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया।
- अमर साहित्यकार का दर्जा: आज, उन्हें हिंदी साहित्य के “अमर साहित्यकारों” में गिना जाता है।
- विरासत: उनकी सबसे बड़ी विरासत है छायावाद की स्थापना और हिंदी साहित्य को एक नई संवेदनशीलता, दार्शनिकता और मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करना। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नया मंच दिया और खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
15 नवंबर, 1937 को, मात्र 48 वर्ष की आयु में, क्षय रोग (Tuberculosis) के कारण वाराणसी में उनका निधन हो गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)
प्रश्न 1: जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षेप में क्या है?
उत्तर: जयशंकर प्रसाद (1889-1937) आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रवर्तक कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। वाराणसी में जन्मे, उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद स्वाध्याय से गहन ज्ञान प्राप्त किया और ‘कामायनी’ जैसे महाकाव्य तथा ‘चंद्रगुप्त’ और ‘स्कंदगुप्त’ जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की।
प्रश्न 2: जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक क्यों कहा जाता है?
उत्तर: क्योंकि वे उन शुरुआती और सबसे प्रमुख कवियों में से थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में छायावाद की मुख्य विशेषताओं – व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रकृति का मानवीकरण, कल्पना की प्रधानता, और दार्शनिक गहराई – को सफलतापूर्वक स्थापित किया। उनकी कृति ‘झरना’ (1918) को अक्सर छायावाद की पहली प्रयोगशाला माना जाता है।
प्रश्न 3: ‘कामायनी’ का मुख्य संदेश क्या है?
उत्तर: ‘कामायनी’ का मुख्य संदेश है कि मानव जीवन में सच्ची शांति और आनंद केवल बुद्धि (इड़ा) या केवल हृदय (श्रद्धा) का अनुसरण करने से नहीं मिलता, बल्कि दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित करने से मिलता है।
निष्कर्ष: एक साहित्यिक युग-प्रवर्तक
जयशंकर प्रसाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण साहित्यिक युग का नाम हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को उस गहराई, दर्शन और कलात्मक उत्कृष्टता से परिचित कराया, जिसकी पहले कमी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि आत्मा का अन्वेषण भी है।
उनका जीवन त्रासदियों से भरा था, लेकिन उनकी कलम ने उन आंसुओं को मोतियों में बदल दिया। आज, दशकों बाद भी, उनकी रचनाएँ प्रासंगिक हैं, प्रेरणा देती हैं, और हमें मानव होने के गहरे अर्थ पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। वे वास्तव में, हिंदी साहित्य के एक अमर हस्ताक्षर हैं।
आपको जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना सबसे अधिक प्रिय है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें!


